कबीर दास की भक्ति भावना के प्रमुख तत्व और विशेषताएँ कबीरदास जितने लोक के निकट है उतने ही भक्ति भावना में गहरे एवं पूर्ण । वे रामानन्द के शिष्य थे और
कबीर दास की भक्ति भावना के प्रमुख तत्व और विशेषताएँ
कबीरदास जितने लोक के निकट है उतने ही भक्ति भावना में गहरे एवं पूर्ण । वे रामानन्द के शिष्य थे और रामानन्द सुगणोपासना के निष्ठावान अनुयायी, फिर भी उन्होंने निर्गुण भक्ति-भावना को अद्वैत तत्त्व से युक्त किया। भक्तिकाल की निर्गुण धारा के सन्त कवि कबीर ने नाथ- पन्थियों की हठयोग साधना में 'भक्ति-भावना' का समावेश कर उसकी नीरसता को सरसता में परिवर्तित कर दिया। भक्त कबीर वैष्णवों के प्रति आदरभाव रखते थे। भक्ति-भावना के लिए द्वैत आवश्यक है, जो सगुणोपासना में ही सम्भव है, क्योंकि निर्गुणोपासक तो आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर अधिक बल देते हैं। इसलिए कबीर की भक्तिभावना सूर तुलसी जैसी नहीं है। कबीर यह स्वीकार करते हैं कि भवसागर से पार जाने # का साधन भक्ति है। कबीर की भक्ति-भावना के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित है-
नाम स्मरण
अधिकांश भक्तों ने प्रभु नाम स्मरण की महत्ता का गुणगान किया है। कबीर भी 'रामनाम' की महिमा का बखान करते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे लिए तो 'नाम' ही खेती-बारी है, नाम ही मेरी धन सम्पदा है, नाम-जप ही मेरी सेवा-पूजा है तथा नाम ही मेरा बन्धु-बान्धव है यथा-
नांउ मेरी खेती नांउ मेरी बारी । भगति करौं जन सरनि तुम्हारी ।
नांउ मेरी माया नांउ मेरी पूजी । तुमहिं छांड़ि जानौ नाहिं दूजी ।।
नांउ मेरी सेवा नांउ मेरी पूजा। तुम्ह बिन और न जानो दूजा ।।
कबीरदास जी का अपना विचार है कि जब एकाग्रचित होकर ईश्वर के नाम का जप किया जाता है, तभी वह फलदायी होता है। वे ऐसे नाम स्मरण का विरोध करते हैं, जिसके कारण मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है-
माला तौ कर में फिरै जीभ फिरै मुख मांहि ।
मनुवां तौ दस दिसि फिरै सो तौ सुमिरन नांहि । ।
कबीर प्रभु नाम का स्मरण लगातार करने की अपील करते हैं। उनका मानना है कि बार-बार पुकारने से कभी तो प्रभु हमारी पुकार सुनेंगे-
केशव कहि-कहि कूकिए न सोइए असरार ।
रात दिवस के कूँकणै कबहुँ लगे पुकार ।।
गुरु महिमा की महत्ता
गुरु का अभिप्राय होता है- मार्गदर्शक। अज्ञानता के अन्धकार को गुरु कृपा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। गुरु-महिमा को कबीर के परवर्ती कवियों ने भी स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि-
'गुरु बिन होइ न ग्यान ।'
कबीर के काव्य में गुरु महिमा का सम्यक् निरूपण हुआ है। उन्होंने कहा कि- 'सतगुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपगार।' उनका मानना है कि गुरु के द्वारा ही 'राम-नाम' रूपी महामन्त्र की प्राप्ति हुई है, जिसकी ज्योति निरन्तर शरीर में जगमगाती रहेगी। गुरु महिमा के बारे में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि- 'ग्यान प्रकास्या गुरु मिल्या सो जनि बीसरि जाइ'। गुरु के बिना साधक सफलतापूर्वक साधना-पथ पर नहीं चल सकता है-
चौसठि दीवा जोरि करि, चौदह चंदा माहि।
तिहिं घर किमि कौ चांदनी, जिहिं घर सतगुरु नाहिं ।।
अर्थात् बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा अज्ञानता समाप्त नहीं हो सकती और तब तक परमात्मा का साक्षात्कार सम्भव नहीं हो सकता।
आचरण की शुद्धता
कबीर ने अपनी भक्तिभावना में सदाचरण पर बल दिया है। वे सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग स्वीकारते हैं। आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को सम्पूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा। विकारों के जनक है कंचन और कामिनी- इनके त्याग से ही सदाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। उनका मानना है कि नारी के कारण ही व्यक्ति, भक्ति, मुक्ति एवं ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता।
नारि नसावै तीनि सुख जा नर पासै होय ।
भगति मुकति निज ज्ञान में पैसि न सकई कोय ।।
कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंग का त्याग करने एवं सत्संग करने पर बल दिया है। उनका विचार है कि जब तक मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या-द्वेष आदि विकार भरे हैं, तब तक हृदय में भगवान् की भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अहंकार एवं त्याग का भी परित्याग करना पड़ता है। 'मैं' का भाव ही अहंकार है। 'मैं' के समाप्त होने पर ही 'तू' अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति सम्भव हो पाती है-
जब मैं था तब तू नहिं अब तू है मैं नाहि ।
सब अंधियारा मिटि गया जब दीपक देख्या मांहि ।।
भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कपट का परित्याग करना पड़ता है। यदि कोई कपटपूर्ण भक्ति करता है तो अन्त में उसे बहुत दुःख झेलना पड़ता है-
कपट की भगति करै जिन कोई।
अन्त की बेर बहुत दुःख होई ।।
प्रपत्ति भाव
प्रपत्ति का तात्पर्य होता है- आत्मनिवेदन प्रस्तुत करना। उनकी भक्ति में प्रपत्ति के सारे आदर्श विद्यमान है। उनका अटूट विश्वास है कि मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ करता है सब ईश्वर करता है -
ना कछु किया न करि सका, ना करणे जोग सरीर ।
जो कछु किया सु हरि किया, तापै भया कबीर-कबीर ।।
कबीर भगवान् की सर्वशक्तिमान मानकर उसकी शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं-
कबीर तेरी सरनि आया, राखि लेहु भगवान ।
मृत्यु का भय भी ईश्वर की शरण में जाने पर ही छूट जाता है। यथा-
भौ सागर अथाह जल तामें बीहित राम अधार।
कहैं कबीर हम हरि सरन् तब गोपद खुर विस्तार । ।
ईश्वर की शरण में जाने पर भव सागर का अथाह जल गोपद से बने गढ़ डे में भरे जल की भाँति सुगमता से पार किया जा सकता है।
ईश्वर में विश्वास
कबीरदास ईश्वर की सर्वशक्तिमान मानते हैं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्त्व है। कबीर को पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वह राई को पर्वत एवं पर्वत को राई करने की सामर्थ्य रखता है, यथा-
साई यूं सब होत है बन्दे पै कछु नाहि।
राई ते परबत करै, परबत राई माहि।।
कबीर यह स्वीकारते हैं कि मानव परमात्मा की कृपा से ही कुछ कर सकने योग्य बनता है। कबीर का यह विश्वास उनकी भक्ति का एक प्रमुख अंग है।
वैराग्य भावना
जो व्यक्ति भक्ति का आकांक्षी है, उसे संसार के प्रति विरक्त भाव अपने मन में जगाना आवश्यक है। वैराग्य का आशय संसार को त्यागकर जंगल में निवास करना नहीं है। संसार में रहते हुए भी मन में संतोष वृत्ति लाना, विषय भोगों के प्रति अनासक्त होना, आशा तृष्णा से मुक्त होना ही वैराग्य है। जब भक्त भगवानौन्मुख हो जाता है, तो सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति स्वतः जाग्रत हो जाती है। कबीर का विचार है कि आशा और तृष्णा जन्म-जन्मान्तर तक पीछा करती रहती है-
माया मरी न मन मुआ मरि-मरि जात सरीर ।
आसा त्रिस्ना ना मरी सौ कहि गये दास कबीर।।
कबीरदास संसार के रिश्ते-नातों को क्षण-भंगुर मानते हैं। सारे सम्बन्ध स्वार्थमय है ऐसा कहकर कबीर वैराग्य जगाने का प्रयास करते हैं-
काकी माता पिता कह काको कौन पुरुष की जोई।
घट फूटै कोठ बात न पूछे काढह कादह होई । ।
अर्थात् वे सांसारिक रिश्ते-नातों में विश्वास नहीं करते हैं।
माधुर्य भाव की भक्ति
माधुर्य भाव की भक्ति को मधुराभक्ति या प्रेम लक्षणा-भक्ति कहा जाता है। भक्त स्वयं को जीवात्मा एवं भगवान् को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ करता है वहाँ मधुरा-भक्ति मानी जाती है। जीवात्मा परमात्मा के विरह का अनुभव करती हुई उससे मिलन की आकांक्षा करती है। कबीर की आत्मा रूपी सुन्दरी बार-बार हरि को अपना 'प्रियतम' मानती हुई कहती है कि 'हरि' के बिना मैं रह नहीं सकती-
हरि पैरा पीव हरि मेरा पीव । हरि बिन रहिन सकै मेरा जीव।।
आत्मा-परमात्मा के मिलन के आनन्द का वर्णन भी कबीर ने विवाह के सॉंगरूपक द्वारा किया है-
दुलहिनि गावहु मंगलचार ।
मोरे घर आये हो राजा राम भरतार ।।
दास्य भाव की भक्ति
तुलसीदास की भक्ति की तरह ही कबीर की भक्ति भावना में भी दास्य भाव दिखाई पड़ता है। वे प्रभु को स्वामी एवं स्वयं को 'दास' सेवक या गुलाम कहते हैं। यथा-
- मैं गुलाम मोहि बेचि गोसाईं ।
- जो सुख प्रभु गोविन्द की सेवा, सो सुख राज न लहियो ।
- दास कबीर भजि सारंग पान, देहु अभय पद मांगौ दान ।।
- कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम।
कबीर भले ही निर्गुण मार्गी भक्त कवि हों, किन्तु उनमें दास्यभाव की भक्ति दिखाई देती है ।
नवधा भक्ति
कबीर के काव्य में नवधा-भक्ति के तत्त्व, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन भी उपलब्ध होते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-
- नाम स्मरण - राम जपौ जिय ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रह्लाद जप्यौ हरि जैसे।
- पाद सेवन - राम चरन मन भाए रे ।
- अर्चन - ऐसी आरती त्रिभुवन वारै। तेज पुंज तहं प्रान उतारै ।
- वन्दन- वन्दे तोहिं वंदिगी सौंकाम। हरि बिन जानि और हराम ।।
- दास्य- सो सेवक जो लाया सेव। तिनहीं पाये निरंजन देव ।
- आत्मनिवेदन- जो है जाका भावता जदि तदि मिलसी आई। जाक तन मन सौंपिया सो कबहूँ छाड़ि न जाइ । ।
भक्त अपने सर्वस्व का समर्पण प्रभु के प्रति करता हुआ कामना-हीन हो जाता है। उसे अपने लिये कोई आकांक्षा नहीं रहती ।
संक्षेपत: कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ एवं अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकाण्ड, अमानवीयता, हिंसा, पर-पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूक पन है वह भी इसी भक्तिभावना के कारण है।







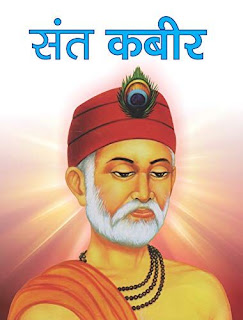

COMMENTS