हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा pdf हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा Hindi Sahitya Itihas Lekhan Ki Parampa
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा pdf हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा Hindi Sahitya Itihas Lekhan Ki Parampara Itihaas lekhan ki parampara Hindi sahitya itihas notes - यद्यपि उन्नीसवीं सदी से पूर्व ही 'चौरासी वैष्णवन की वार्त्ता', 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्त्ता', 'भक्तमाल', 'गुरुग्रन्थसाहब', 'गोसाईं चरित्र', 'भक्तनामावली', 'कविमाला', 'कालिदास हजारा' तथा 'सत्कविगिरा विलास' जैसे अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हो चुका था, जिनमें हिन्दी के विभिन्न कवियों के जीवनवृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है।किन्तु इनमें कालक्रम, सन्-संवत् आदि का अभाव होने के कारण इन्हें 'इतिहास' की संज्ञा नहीं दी जा सकती।
हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक
ज्ञात तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान् गार्सा द तॉसी ने किया है। इनके ग्रन्थ का नाम है- 'इस्त्वार द ला लितरेत्युर ऐंदुई ऐ ऐंदुस्तानी'। यह ग्रन्थ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें हिन्दी और उर्दू के अनेक कवियों का विवेचन वर्णक्रमानुसार किया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 ई. में तथा द्वितीय भाग 1847 ई. में प्रकाशित हुआ था। इसके द्वितीय संस्करण को संशोधित एवं परिष्कृत करके 1871 ई. में प्रकाशित कराया गया। इसमें 3 खण्ड हैं। तॉसी की परम्परा को प्रवर्द्धित करने का प्रयास शिवसिंह सेंगर ने किया। इनके ग्रन्थ का नाम 'शिवसिंह सरोज' है। यह हिन्दी साहित्येतिहास-लेखन-परम्परा का द्वितीय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह 1883 ई. में प्रकाशित हुआ था। इसमें लगभग एक हजार भाषा-कवियों का जीवन-चरित उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रन्थ में प्रयुक्त सामग्री विश्वसनीय नहीं है। इसलिये इसकी ऐतिहासिकता खतरे में पड़ जाती है। इस ग्रन्थ का महत्त्व इतना ही है कि इससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय तक उपलब्ध हिन्दी कविता सम्बन्धी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है।
उपर्युक्त दोनों ग्रंथों के बाद जार्ज ग्रियर्सन की कृति 'द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' का नाम आता है। इसका प्रकाशन 1888 ई. में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में हुआ। यद्यपि इस कृति के नाम में कोई ऐतिहासिकता नहीं झलकती है, फिर भी इसे हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त ने ग्रियर्सन की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि- "वस्तुत: उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण में जबकि हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परम्पराओं का श्रीगणेश भी न हुआ था, हिन्दी-भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक-ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा-शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रन्थ अँगरेज़ी में रचित होने के कारण हिन्दी के अध्येताओं की दृष्टि का केन्द्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार, जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिन्दी माध्यम से प्रस्तुत कर सकें, उस यश के भागी बनें, जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था।"
जॉर्ज ग्रियर्सन की उपर्युक्त कृति के अनंतर मिश्र बन्धुओं का 'मिश्रबन्धुविनोद' नामक ग्रन्थ प्रकाश में आया। चार भागों में विभक्त इस कृति के प्रथम तीन भाग 1913 ई. में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ई. प्रकाशित हुआ। यद्यपि मिश्रबन्धुओं ने इसे इतिहास ग्रन्थ की संज्ञा नहीं दी है, किन्तु इसे आदर्श इतिहास ग्रन्थ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसमें इतिहास-लेखन की आलोचनात्मक प्रणाली के प्रयोग के साथ-साथ साहित्य के विविधांगों का भी विवेचन मिलता है यह एक बृहदाकार ग्रंथ है। हिन्दी के लगभग पाँच हजार कवियों का परिचय इसमें समाविष्ट है। यह कृति आठ से भी अधिक खण्डों में विभाजित है। यह कृति परवर्ती इतिहासकारों के लिए आधार-ग्रन्थ सिद्ध हुई। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की स्वीकारोक्ति है कि- "कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय: 'मिश्रबन्धुविनोद' से ही लिये हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास सम्बन्धी प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार
हिन्दी साहित्य के इतिहास की परम्परा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा रचित 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (1929 ई.) को प्राप्त है, जो वस्तुत: काशी - नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी शब्दसागर' की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्द्धित एवं विस्तृत करके स्वतन्त्र ग्रन्थ का रूप दिया गया। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की दृष्टि अधिक व्यापक, स्पष्ट, सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक है।
आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा है- "जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। "
हिन्दी साहित्य के चार काल कौन कौन से हैं?
हिन्दी साहित्य के इतिहास का प्रामाणिक और उत्कृष्ट काल-विभाजन सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल का मिलता है। अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी मानकर काल विशेष में ग्रंथों की प्रसिद्धि और प्रचुरता को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने 1000 वर्षों के हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बाँटा गया है-
- आदिकाल या वीरगाथाकाल (सं. 1050-1375 तक)
- पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल (सं. 1375-1700 तक)
- उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल (सं. 1700-1900 तक)
- आधुनिककाल या गद्यकाल (सं. 1900-1984 तक) ।
आचार्य शुक्ल के उपरान्त यदि किसी अन्य विद्वान् की मान्यताओं को हिन्दी जगत् ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है, तो वे आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ही हैं जिन्होंने आदिकाल के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य किया है। अब तक साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उनकी निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाश में आयी है-
- हिन्दी साहित्य की भूमिका
- हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास
- हिन्दी साहित्य का आदिकाल ।
आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिन्दी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास-ग्रन्थ नहीं है, परन्तु उसमें दिये गये स्वतन्त्र लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन हेतु नयी सामग्री एवं नयी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त ने आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के योगदान पर चर्चा करते हुए लिखा है- " वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खण्डित किया । ... जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परम्परा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिन्दी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं।
उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य अनेक इतिहास-ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। इनमें बाबू श्यामसुन्दर दास कृत 'हिन्दी-भाषा और साहित्य', डॉ. सूर्यकान्त शास्त्री रचित 'हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास', पं. कृष्णशंकर शुक्ल कृत' आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास', अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रणीत 'हिन्दी-भाषा और उसके साहित्य का विकास', डॉ. वर्मा रचित 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', आचार्य नलिनविलोचन शर्मा लिखित रामकुमार 'साहित्य का इतिहास-दर्शन', डॉ. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', डॉ. धीरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य' आदि प्रसिद्ध हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन को पूर्णता प्रदान करने के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 'हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास' प्रकाशित किया है।







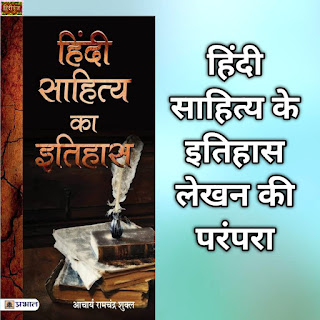

Hindi sahity hitihas lekhan ki parampara ko aspsat kijiye
जवाब देंहटाएंHindi sahity hitihas lekhan ki parampara ko aspsat kijiye
जवाब देंहटाएंHindi sahitya itihas lekhan ki parmpra ko aspst kijiye
जवाब देंहटाएं